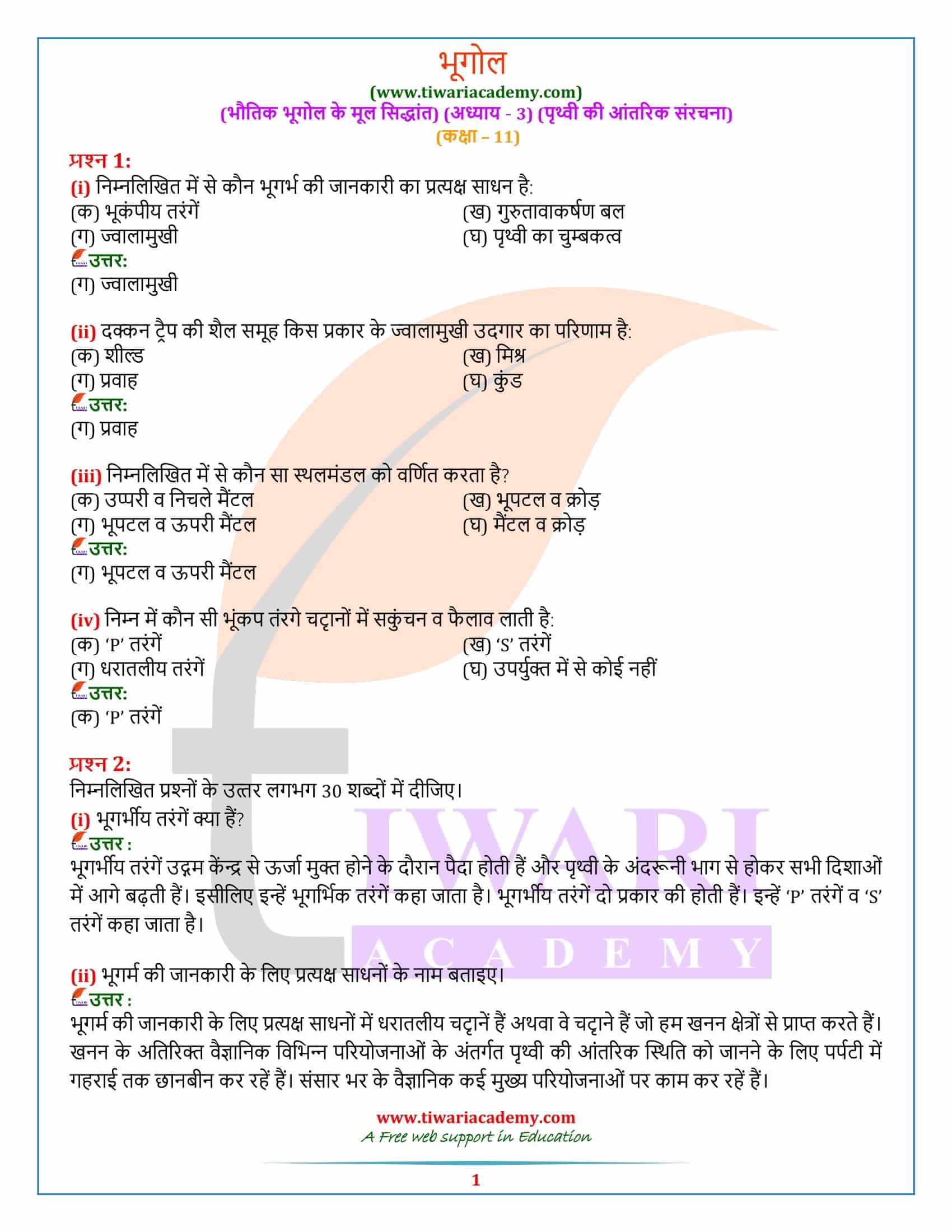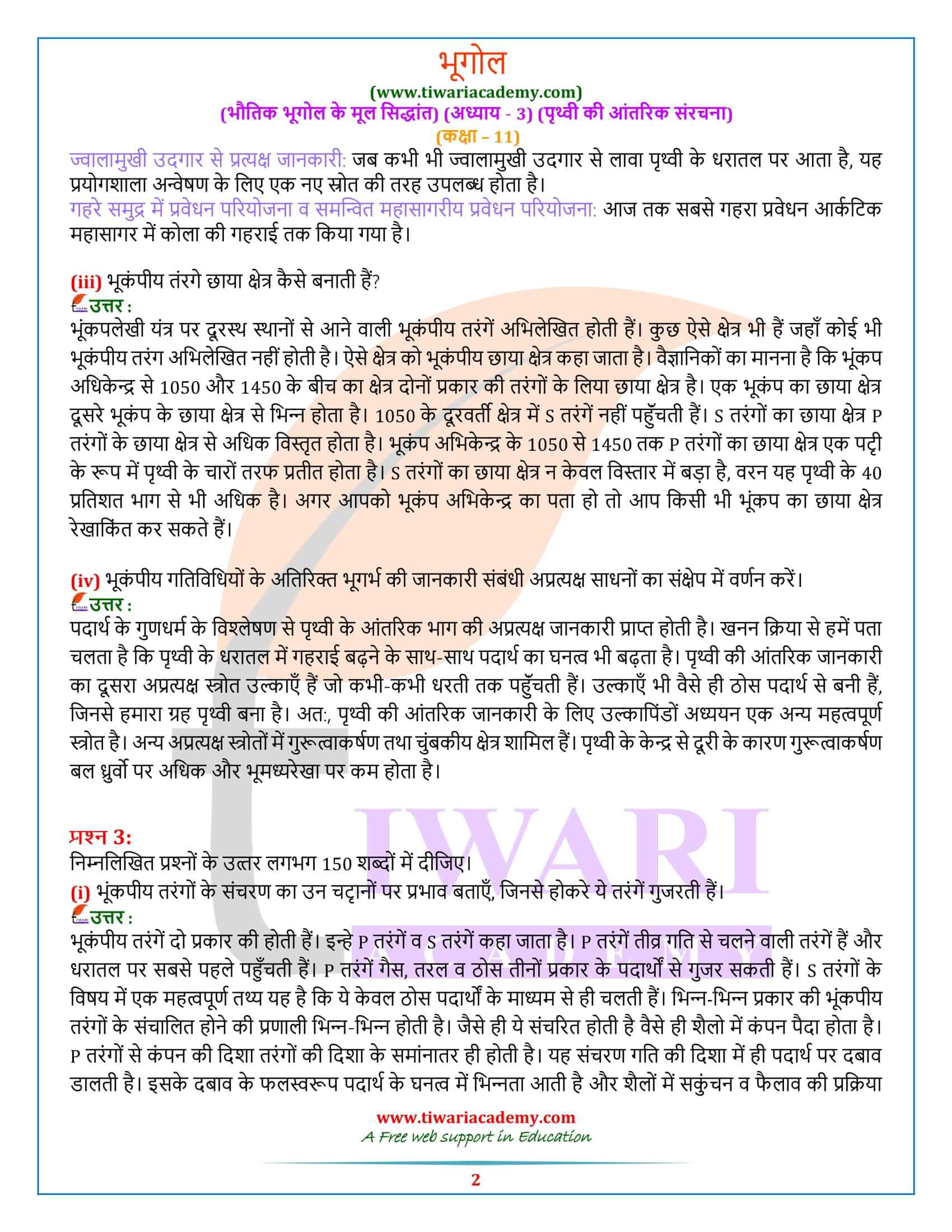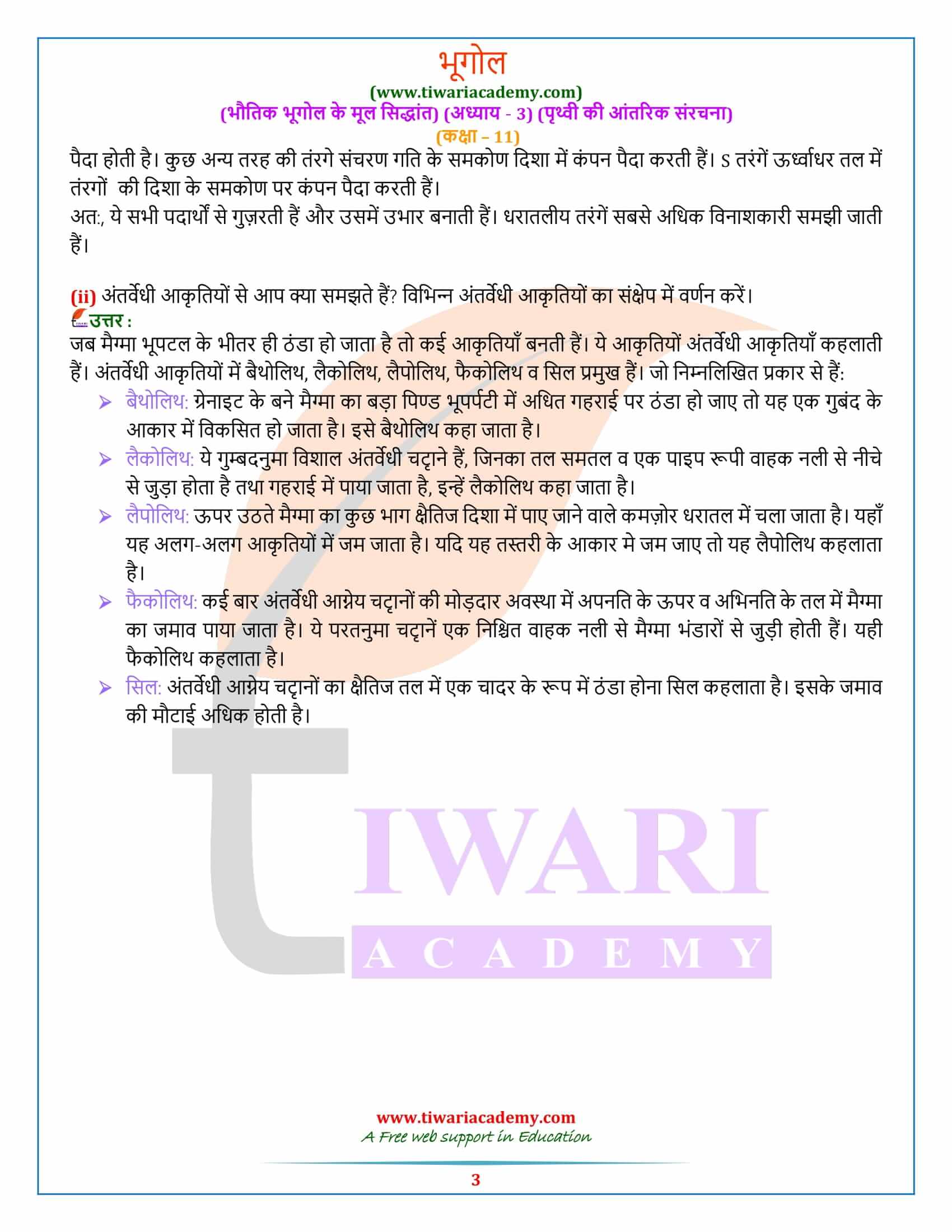एनसीईआरटी समाधान कक्षा 11 भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना
एनसीईआरटी समाधान कक्षा 11 भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के सवाल जवाब सत्र 2025-26 के अनुसार संशोधित रूप में यहाँ से मुफ्त प्राप्त किए जा सकते हैं। कक्षा 11 भूगोल पाठ 3 पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के इकाई II पृथ्वी के सभी उत्तर यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए हैं।
एनसीईआरटी समाधान कक्षा 11 भूगोल अध्याय 3
कक्षा 11 भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रश्न उत्तर
भूगर्म की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए।
भूगर्म की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों में धरातलीय चटृानें हैं अथवा वे चटृाने हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर रहें हैं। संसार भर के वैज्ञानिक कई मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहें हैं।
ज्वालामुखी उदगार से प्रत्यक्ष जानकारी: जब कभी भी ज्वालामुखी उदगार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए एक नए स्रोत की तरह उपलब्ध होता है।
गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना: आज तक सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला की गहराई तक किया गया है।
भूगर्भीय तरंगें क्या हैं?
भूगर्भीय तरंगें उद्गम केंन्द्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। इसीलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। इन्हें P तरंगें व S तरंगें कहा जाता है।
कक्षा 11 भूगोल अध्याय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है:
दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उदगार का परिणाम है:
निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है?
निम्न में कौन सी भूंकप तंरगे चटृानों में सकुंचन व फैलाव लाती है:
भूकंपीय तंरगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं?
भूंकपलेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूंकप अधिकेन्द्र से 1050 और 1450 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिया छाया क्षेत्र है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। 1050 के दूरवर्ती क्षेत्र में S तरंगें नहीं पहॅुंचती हैं। S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। भूकंप अभिकेन्द्र के 1050 से 1450 तक P तरंगों का छाया क्षेत्र एक पटृी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। S तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40 प्रतिशत भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अभिकेन्द्र का पता हो तो आप किसी भी भूंकप का छाया क्षेत्र रेखाकिंत कर सकते हैं।
भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन करें।
पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ-साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्त्रोत उल्काएँ हैं जो कभी-कभी धरती तक पहॅुंचती हैं। उल्काएँ भी वैसे ही ठोस पदार्थ से बनी हैं, जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अत:, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्कापिंडों अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्त्रोतों में गुरूत्वाकर्षण तथा चुंबकीय क्षेत्र शामिल हैं। पृथ्वी के केन्द्र से दूरी के कारण गुरूत्वाकर्षण बल ध्रुर्वो पर अधिक और भूमध्यरेखा पर कम होता है।
भूंकपीय तरंगों के संचरण का उन चटृानों पर प्रभाव बताएँ, जिनसे होकरे ये तरंगें गुजरती हैं।
भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। इन्हे P तरंगें व S तरंगें कहा जाता है। P तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। P तरंगें गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। S तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार की भूंकपीय तरंगों के संचालित होने की प्रणाली भिन्न-भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है वैसे ही शैलो में कंपन पैदा होता है। P तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांनातर ही होती है।
यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में सकुंचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। कुछ अन्य तरह की तंरगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। S तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तंरगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं।
अत:, ये सभी पदार्थों से गुज़रती हैं और उसमें उभार बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं।
अंतर्वेधी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेधी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करें।
जब मैग्मा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियॉं बनती हैं। ये आकृतियों अंतर्वेधी आकृतियॉं कहलाती हैं। अंतर्वेधी आकृतियों में बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ व सिल प्रमुख हैं। जो निम्नलिखित प्रकार से हैं:
बैथोलिथ: ग्रेनाइट के बने मैग्मा का बड़ा पिण्ड भूपर्पटी में अधित गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुबंद के आकार में विकसित हो जाता है। इसे बैथोलिथ कहा जाता है।
लैकोलिथ: ये गुम्बदनुमा विशाल अंतर्वेधी चटृाने हैं, जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है तथा गहराई में पाया जाता है, इन्हें लैकोलिथ कहा जाता है।
लैपोलिथ: ऊपर उठते मैग्मा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग-अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार मे जम जाए तो यह लैपोलिथ कहलाता है।
फैकोलिथ: कई बार अंतर्वेधी आग्नेय चटृानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में मैग्मा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा चटृानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। यही फैकोलिथ कहलाता है।
सिल: अंतर्वेधी आग्नेय चटृानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। इसके जमाव की मौटाई अधिक होती है।